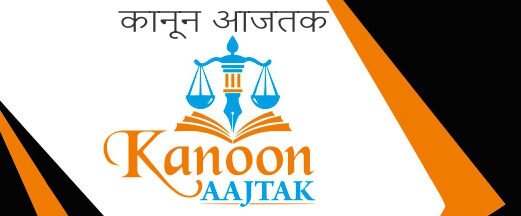आगरा/नई दिल्ली 26 दिसंबर ।
जस्टिस ई एस वेंकटरमैया शताब्दी व्याख्यान 2024 में ‘संवैधानिक संस्था की पुनर्कल्पना: दक्षता, अखंडता और जवाबदेही’ पर बोलते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने बताया कि सेवा मामलों में बढ़ते मुकदमेबाजी ने लोक सेवाओं में चयन की गुणवत्ता की समीक्षा करने की आवश्यकता का संकेत दिया है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोक सेवकों की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेहतरी के लिए था, लेकिन अब यह प्रवृत्ति उभरी है कि राज्य केवल लोक सेवकों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है।
उन्होंने कहा :
“यदि हम खुद से यह सवाल पूछें कि क्या लोक सेवा राज्य के हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई है या राज्य लोक सेवकों के हितों की पूर्ति कर रहा है, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकारी नौकरी अपने आप में एक लक्ष्य बन गई है।”
“इस स्थिति ने छोटे-छोटे मुद्दों पर भारी मुकदमेबाजी को जन्म दिया है, जिससे वरिष्ठता, पदोन्नति, स्थानांतरण, नियमितीकरण आदि के विवाद पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि लोक सेवा आयोग इस विसंगति या असंतुलन पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि आधुनिक भारत में नौकरशाही में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा, ईमानदार और दूरदर्शी लोग हों, जो दुनिया भर में किसी के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण बन सकें।”
दूसरी ओर, जस्टिस नरसिम्हा ने भारत में चुनाव आयोग की बहुलतावादी प्रणाली के सार की सराहना की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित न हो।
उन्होंने कहा:
“आज हमारे पास एक ऐसा चुनाव आयोग है जिसमें विचारों की बहुलता है, जो मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले निर्णय लेने से कहीं बेहतर है। हम अक्सर चुनाव आयोग के तीन सदस्यों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्र को संबोधित करते हुए देखते हैं। यह संस्था के साथ काम करने का एक सकारात्मक तरीका है। इससे आयोग को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मान्यता मिली है। यह लोकतंत्र की परिपक्वता का सूचक है, जहां हमने एक संस्था की क्षमता का प्रयोग और संवर्धन किया है।”
यहां, जस्टिस नरसिम्हा चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यापार का लेन-देन) अधिनियम, 1991 के माध्यम से दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त रखने के प्रावधान का उल्लेख कर रहे थे।
Also Read – यूपी की बरेली कोर्ट ने अपने ही भाई की हत्या के आरोपी पिता पुत्र को सुनायी मौत सजा

उल्लेखनीय है कि टीएन शेषन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा और वरिष्ठ वकील नानी पालकीवाला के इस तर्क को खारिज कर दिया कि तीन चुनाव आयुक्तों के होने से निर्णय लेने में थकान और प्रशासनिक कठिनाइयां होंगी।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण वाद निस्तारण को प्राथमिकता दे
हालांकि, जस्टिस नरसिम्हा ने राज्य चुनाव आयोगों द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने पर भी चिंता जताईः
“मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने का अतिरिक्त भार राज्य चुनाव आयोगों पर डाला गया है। उनके कामकाज को लेकर चिंताएं हैं, जिनका समाधान न केवल चुनाव आयोग को करना चाहिए, बल्कि विधानसभाओं, सरकारों और अदालतों पर भी समान जिम्मेदारी है।”
जस्टिस नरसिम्हा ने चुनाव आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी और सूचना आयोग जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के महत्व को समझाया, जो अन्य लोकतांत्रिक पारंपरिक संस्थाओं को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी संस्थाएं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनती हैं- ‘चौथी शाखा संस्थाएं’।
विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ब्रूस एकरमैन ने ऐसी संस्थाओं को ‘ईमानदार संस्थाएं’ कहा है, जो राजनीतिक प्रभाव की अभिव्यक्ति हैं।
उन्होंने विभिन्न प्रोफेसरों और विद्वानों द्वारा गढ़े गए अन्य शब्दों के बारे में विस्तार से बताया:
“दूसरी ओर, प्रोफेसर मार्क टशनेट ने दक्षिण अफ्रीकी संविधान की शब्दावली उधार ली है और उन्हें संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन और संरक्षण करने वाली संस्थाएं कहा है। हमारे चुनाव आयोग का संदर्भ लें। प्रोफेसर तरुणभ खेतान ने इन संस्थाओं को “गारंटर संस्थाएं” भी कहा है, जो उन्हें संवैधानिक मानदंडों की गारंटी देने और उन्हें लागू करने वाली दर्जी-निर्मित, विशिष्ट और स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं बताते हैं।”
चौथी शाखा संस्थाओं के 3 स्पर्शरेखाएं
जस्टिस नरसिम्हा ने चर्चा की कि ‘चौथी शाखा संस्थाएं 3 तत्वों के कारण ऐसी बनती हैं:
(1) संस्थागत संरचना: यह संदर्भित करती है कि इनमें से कुछ संस्थाएं कैसे बनाई जाती हैं। क्या वे संवैधानिक हैं या विधायी हैं? क्या उनकी संरचना कानून में अंतर्निहित है या संरचना को डिज़ाइन करने के लिए नियम निर्धारित करने के लिए कार्यपालिका है? इन संस्थाओं की संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, पारिश्रमिक, समाप्ति आदि
(2) संस्थागत शैली: यह संदर्भित करती है कि ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया, मानक विनियमों की स्थिति जो उन्हें जवाबदेही से कार्य करने की आवश्यकता होती है।

(3) संस्थागत सार: इन संस्थाओं के कार्यों और कर्तव्यों की विषय-वस्तु, दायरा और सीमा को संदर्भित करता है।
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि जबकि कुछ चौथी शाखा की संस्थाओं की स्थापना संविधान द्वारा ही की गई थी, कुछ अन्य संसदीय विधियों की उपज थे और आज वैधानिक निकायों के रूप में मौजूद हैं जो “विशेष और स्वतंत्र कामकाज के माध्यम से संवैधानिक मानदंडों को पूरा करते हैं, और जिनमें संवैधानिक रूप से स्थापित चौथी शाखा संस्थानों के समान विशेषताएं हैं।”
निष्कर्ष में जस्टिस नरसिम्हा ने 6 कारकों पर ध्यान दिया जो इस बात में योगदान दे सकते हैं कि संस्थान क्यों काम नहीं करते या कम प्रदर्शन करते हैं।
इनमें (1) क्षमता विफलता; (2) अवसंरचना विफलताएं; (3) स्वायत्तता की कमी; (4) प्रवर्तन विफलताएं; (5) राजनीतिक हस्तक्षेप; (6) ओवरलैपिंग जनादेश और समन्वय की कमी शामिल हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
साभार: लाइव लॉ